
प्रतीकों से गांधी के विचारों के कालजयी प्रभाव से नहीं समझा जा सकता

Faisal Anurag प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बीच अहिंसा, सम्मान और सहिष्णुता के गांधी संदेश की जरूरतों के साथ ट्रस्टीशिप के महत्व को रेखांकित किया गया. सभ्यतागत संकट और वैश्विक टकराव के इस दौर में गांधी उम्मीदों के केंद्र बनते जा रहे हैं. गांधी जी का विचार उस मानविक करूणा से ओतप्रोत है जो आज की राजनीति, अर्थनीति और वैश्विक नीति की उग्रता के खिलाफ एक नए प्रतिरोध का आह्वान करता है. दरअसल यही वह नजरिया है जिसे दुनिया भर के शासक नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं. गांधी की अहिंसा को शोषण की लूट से अलग थलग देखने का माहौल बनाया जा रहा है. गांधी सामाजिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ थे, लेकिन आज आर्थिक विषमता को मजबूती देने वाले नेता गांधी को प्रतीक बना कर उनकी जीवंतता से खेलने का प्रयास कर रहे हैं. गांधी को किसी एक उदाहरण या एक घटनाक्रम में नहीं समेटा जा सकता है. गांधी आनेवाले समय को जितनी गहरायी से देखते थे. उतना ही भविष्य के टकरावों को लेकर भी सजग थे. गांधी एक ऐसे समय में उभरे जब जनमानस दिमागी गुलामी के भयावह दौर में था. उससे बाहर निकाल कर भारतीय समाज की विविधताओं और बहुलताओं के बीच उन्हें एकजुट करना कोई सामान्य राजनीतिक अभिक्रम नहीं है. गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रयोग से अनेक सीख हासिल किए. उन्हीं शिक्षाओं ने उन्हें दुनिया भर के परतंत्र देशों का वह प्रेरक स्रोत बनाया जो स्वशासन, बराबरी और बंधुता के सेकुलर विवेक और आधिपत्य वाल सांस्कृतिक परिवेश से मुक्त होने का स्वप्न दिया. यही सपना आज भी असमानता और आर्थिक शोषण के हर प्रवृति और प्रक्रिया के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष की चेतना प्रदान करता है. गांधी को समझने के लिए जरूरी है इंसान की जान की कीमत को समझा जाए और साथ ही धर्म, जाति, जेंडर और नस्ल के भेदभाव को भी. भारत ने आजादी के बाद 75 सालों का सफर तय कर लिया है, लेकिन देश के भीतर आज भी दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समूहों को अपने अस्त्वित्व, असिमता और आत्मसम्मान के साथ हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. अमेरिका में भी यदि ````ब्लैक लाइव मैटर```` ने नस्ली भेदभाव और जुल्म का सवाल उठाया है जो जाहिर है कि लोकतंत्र अब भी वर्चस्ववादी ताकतों की सांस्कृतिक प्रभुत्व से बाहर नहीं निकल पाया है. यही वह द्वंद है जो गांधी की अहिंसा,करूणा और ````पीर पराई```` से आत्मानुभूति के संदर्भ को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करता है. गांधी जी का प्रिय भजन था जिसे नरसिंह मेहता ने लिखा था `` वैष्णवजन को तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे `` इसी में आंतरहित है गांधी का पूरा दर्शन. दरअसल गांधी दूसरों के सिर्फ आत्मिक दुखों से संवेदित नहीं होते थे बल्कि आर्थिक और समाजिक उत्पीड़न भी उन्हें परेशान करता था. इसलिए गांधी ने ट्रस्टीशिप का विचार प्रस्तुत किया. उनका ट्रस्टीशिप वास्तव में गांधी अर्थशास्त्र का अहम सूत्र है जो संपत्तियों की हिस्सेदारी के त्याग पर निर्भर है. गांधी का यह दर्शन वास्तव में मुनाफा आधारित औद्यौगिक संस्कृति का निषेद भी करता है. गांधीवादी समाजवादी किशन पटनायक ने एक लेख में कहा था कि गांधी की कथनी और करनी के व्यापक संसार को समझने की जरूरत है. यही कारण है कि आज की सत्ता गांधी को केवल प्रतीक के बतौर पर समझती है. जब कि विश्व नागरिक उन्हें एक वैकल्पिक सभ्यता के संदर्भ में परिभाषित करते हैं. सत्ताओं ने दुनिया के क्रांतिकारी विचारों को रूपकों यानी मेटाफर और प्रतीकों यानी सिबंल में समेटा है. रिचर्ड एटनबारो की फिल्म गांधी प्रतीकों के इस द्वंद को कुछ दृश्यों में रेखांकित करती है. गांधी जब चंपारण के किसानों के बीच गए तो न केवल पहनावे से बल्कि विचारों और अहिंसा के क्रांतिकारी तेवर को भी नया रूप प्रदान किया. भारत और अमेरिका के किसानों के आज के दर्द के संदर्भ में प्रतीकों की सीमाओं को समझा जा सकता है. लुई फीशर जिन्होंने गांधी की हत्या के पहले बातचीत का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है. गांधी ने फीशर के सवालों के जवाब में कहा था कि वे जमीनों के वितरण के लिए पहले जमीन के मालिकों से आग्रह करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे किसानों और भूमिहीनों के अधिकारों के साथ खड़े हो जाएंगे. भले ही उन्हें अपनी सरकार का विरोध क्यों न करना पड़े. आज के किसान आंदोलन के संदर्भ में भी इसे समझा जा सकता है. गांधी होने का मतलब उत्पीड़नों के तमाम संदर्भ और अधिनायकत्व के तमामा संदर्भो के खिलाफ उठ खड़ा होना है. गांधी की अहिंसा गरीब और कमजोर को उसकी हिस्सेदारी दिलाना है. गांधी धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे. [wpse_comments_template]

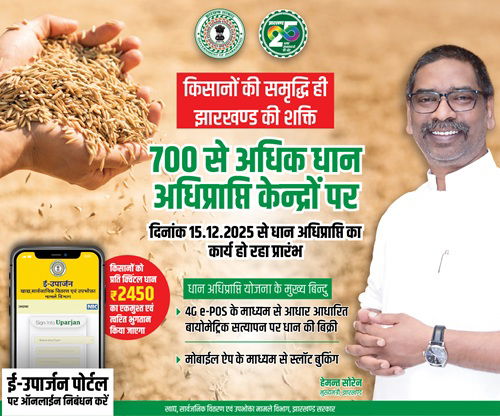

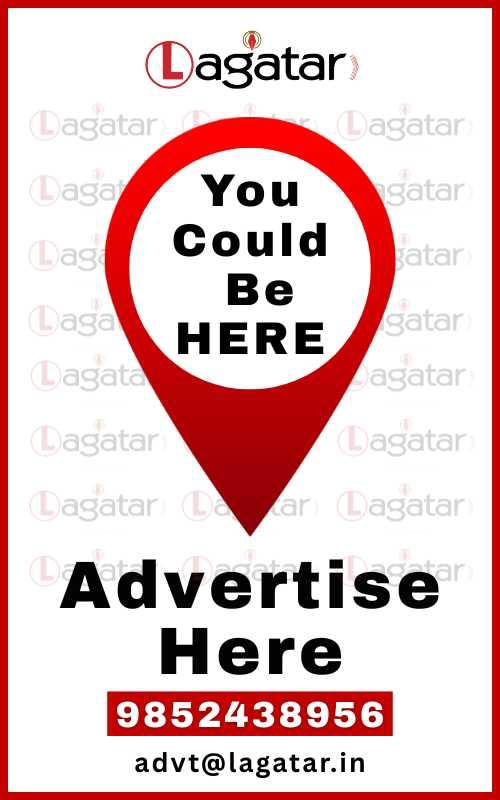
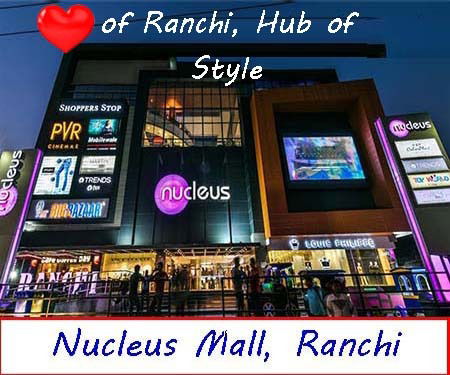
Leave a Comment