
नोबल पुरस्कार में पिछड़े भारत के विश्वगुरू का दंभ से हकीकत नहीं बदल सकती

Faisal Anurag भारत को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913, विज्ञान का 1930, अर्थशास्त्र का 1998 और शांति के लिए 1979 और 2014 में ही हासिल हुआ. भारतीय मूल के चार विदेशी नागरिकों को भी क्रमश:1968,1983,2009 और 2019 नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है. इनमें तीन विज्ञान के लिए और एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए. सवाल यह है कि आखिर भारत में रहने और शोध करने वाले वैज्ञानिक विश्व के सबसे मशहूर पुरस्कार हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं. जबकि माना जाता है कि भारत के नागरिकों ने दुनिया भर में अपने शोधों और मेहनत का डंका बजाया है. आइटी के क्षेत्र में तो अनेक देशों की निर्भरता भारतीय नागरिकों पर ही है. बावजूद शोध और मौलिक योगदान के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों का पिछड़ जाना बेहद तकलीफदेह अनुभव है. तंजानिया के जांजीबारी अब्दुलरज्जाक गुरनाह को इस बार साहित्य का पुरस्कार दिया गया है. गुरनाह को इसके पहले बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया. गुरनाह दूसरे अफ्रीकी अश्वेत हैं, जिन्हें इस सर्वोच्च पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसके पहले अफ्रीकी साहित्य में क्रांतिकारी प्रयोगों और अफ्रीकी नागरिकों के स्वभिमान, समानता और आत्माधिकार को स्वर देने वाले वोल शोयंका को यह पुरस्कार दिया जा चुका है. अफ्रीकी साहित्य के जानकार विजय शर्मा के अनुसार, `इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जंजीबार में जन्मे तथा इंग्लैंड में रह रहे अब्दुलरज़ाक गुरनाह को दिया गया है. 1996 के बाद अर्थात दो युग के पश्चात यह किसी अश्वेत लेखक को मिला है. 1996 में यह अमेरिकी अश्वेत लेखिका टोनी मॉरीसन को प्राप्त हुआ था. इन दोनों को बुकर पुरस्कार भी मिला है. दोनों के एक उपन्यास का नाम एक है, ‘पैराडाइज’ (हालांकि दोनों का कथानक बिल्कुल भिन्न है ). लंबे समय तक नोबेल समिति ने किसी अन्य अश्वेत लेखक को पुरस्कार के योग्य न समझा जबकि कई अश्वेत लेखक जैसे न्युगी व थियांगो इसके हकदार हैं.` गुनरनाह मूलत: स्वाहिली भाषा बोलते हैं. पहले वे इसी भाषा में लिखते थे, बाद में उन्होंने केवल अंग्रेजी में लेखन किया है. न्गुगी वा थ्योंगो की कहानी ठीक इसके उलट है वे कीनिया के रहने वाले हैं. पहले वे अंग्रेजी में लेखन कर ही मशहूर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लोगों की भाषा गिकियू में लिखना शुरू किया. उनका अधिकांश श्रेष्ठ साहित्य और वैचारिक लेखन इसी भाषा में हुआ है. भारत में भी बेहद लोकप्रिय है. भारत की अनेक भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है. गुरनाह ने औपनिवेशिक और शरणार्थी अनुभव पर ही अपने लेखन को केंद्रित किया है. भारत को साहित्य का पहला और अब तक का एकमात्र नोबल रवींद्रनाथ टैगोर को उस दौर में मिला, जब भारत गुलाम था और आजादी के लिए अंगड़ाई ले रहा था. टैगोर का सारा लेखन बंगाली में है. दुनिया के लगभ्ग 75 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं. भारत के बाहर भी हिंदी लेखकों की फौज है. इसमें मॉरीशस,फीजी,गुयाना जैसे देश शामिल हैं. लेकिन नोबल पुरस्कार के 121 सालों के इतिहास में एक भी हिंदी लेखक का नाम भी विचारार्थ नहीं माना गया है. दुनिया में बेहद कम संख्या में बोली लिखी जाने वाली भाषाओं के लेखकों ने भी सारी दुनिया में अपने विषय और लेखन की बहुलता और प्रतिबद्धता के सहारे लोहा मनवाया है. लेकिन वह क्या कारण है कि हिंदी साहित्य की दुनिया के विषयों में समय,समाज,इतिहास,औपनिवेशिक दासता के दर्द हो या आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुई असमानता के सवाल हिंदी तो छोड़ दें, भारत की अन्य भाषाओं के लेखन के स्तर पर भी मुकाबला नहीं कर पाते हैं. भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कारों की फेहरिस्त भी खंगाली जा सकती है. 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार में अब तक 10 लेखकों की रचनाओं को ही इसके लिए चुना गया है. यानी 56 सालों में दस पुरस्कार. विज्ञान के क्षेत्र का संकट तो और भी गहरा है. विश्वगुरू होने का दंभ एक ओर है और वास्तविकता दूसरी ओर. भारत के विज्ञान शोधों और अन्वेषण को लेकर दुनिया यदि प्रभावित नहीं हो पाती है, तो इसके सामाजिक संदर्भों के साथ आर्थिक नीतियों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है. विज्ञान के अन्वेषण न केवल किसी देश की गरिमा को बढ़ाते हैं बल्कि वैश्विक स्तर पर उसे विशेष स्थान भी दिलाते हैं. 1930 सी. वी रमण को भौतिकी विज्ञान के लिए यह पुरस्कार मिला. भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना को मेडिसिन,एस चंद्रशेखर जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, को भौतिकी और बेंकी रामाकृष्णन जो कि भारती मूल के ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक हैं, को रसायन विज्ञान के लिए नोबल सम्मान दिया गया. यानी विज्ञान के क्षेत्र में कुल चार. तो यह है भारत की विश्वगुरू की असलियत जिसका 2914 के बाद से लगातार डंका पीटा जा रहा है. टैगोर और रमन के नाम पर कब तक भारतीय ज्ञान विज्ञान का दंभ भरा जाता रहेगा. भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देशों का हाल भी यही है. राजनीति के साथ ही जाति,धर्म और सामंती मिजाज के वर्चस्ववादी की मानसिकता ही वह बाधक है, जो अन्वेषण की मौलिकता और लेखन पर हावी है. [wpse_comments_template]

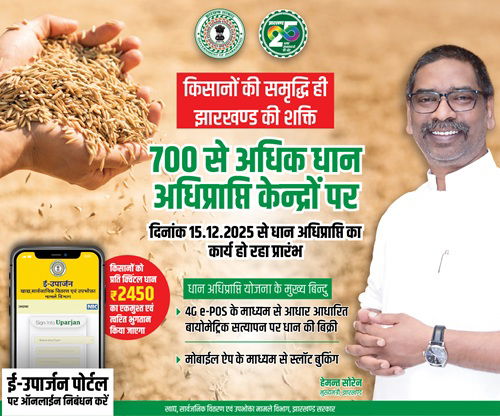

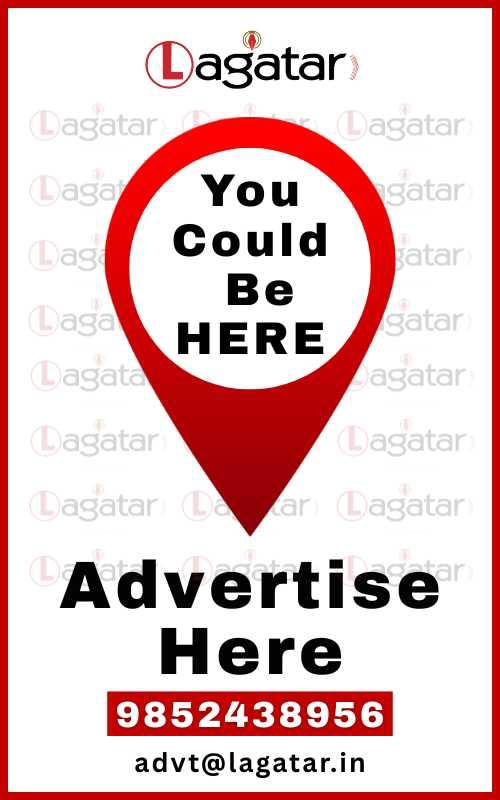
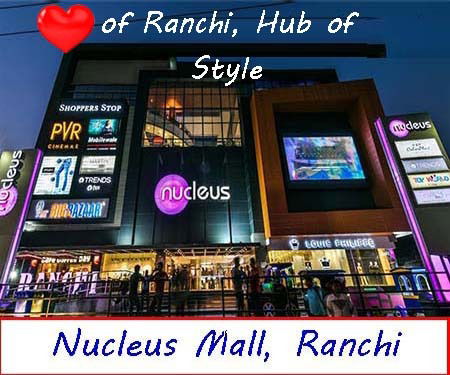
Leave a Comment