देश में गठबंधन की राजनीति

Brijendra Dubey 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाई किसके बीच होगी, इसकी तस्वीर साफ होती दिख रही है. कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है. इसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस है. इस गठबंधन की टैगलाइन जीतेगा भारत रखी गई है. इसके जवाब में भाजपा 38 दलों के साथ एनडीए कुनबा मजबूत करने में जुट गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के 25 साल पूरे होने पर नई परिभाषा दी है. उन्होंने कहा कि एन से न्यू इंडिया, डी से डेवलपमेंट और ए से एस्पिरेशन. इससे साफ हो गया है कि अगला लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया में होगा. ऐसा पहली बार होगा, जब इतनी सारी पार्टियों से मिल कर बने दो गठबंधन आपस में भिड़ेंगे. हालांकि देश में गठबंधन की राजनीति का इतिहास आजादी के कुछ साल बाद से ही शुरू हो जाता है. और केंद्र में भी कई बार गठबंधन सरकारें बन चुकी हैं. 1982 में रोजर स्क्रटन की एक किताब आई थी - अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल थॉट. इस किताब में गठबंधन की परिभाषा दी गई थी. इसके मुताबिक, अलग-अलग पार्टियों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है. आपको याद दिला दें कि भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत राज्यस्तर पर हुई थी. 1953 में आंध्र प्रदेश में गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार मात्र 13 महीने ही चल सकी थी. उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी मिली-जुली सरकारें बनीं. आजादी के बाद लगभग दो दशकों तक तो कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं मिली. हालांकि उस समय दूसरी विचारधारा की पार्टियां जरूर थीं. 1964 में जवाहर लाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद राजनीति भी बदलनी शुरू हो गई. राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की शुरुआत 70 के दशक में शुरू हुई. इस बीच, 1975 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया. उसने विपक्ष को कांग्रेस के खिलाफ साथ आने का मौका दे दिया. अक्टूबर 1951 में जनसंघ का गठन हुआ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए. जनसंघ एक राष्ट्रवादी पार्टी थी. 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में जनसंघ के तीन सदस्य चुने गए. इनमें से एक खुद मुखर्जी थे. उन्होंने ओडिशा (तब उड़ीसा) की गणतंत्र परिषद, पंजाब की अकाली दल, हिंदू महासभा और निर्दलीय सांसदों सहित छोटी-छोटी पार्टियों को मिला कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के नाम से गठबंधन बनाया. इस दल के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे. दल का मकसद तत्कालीन नेहरू सरकार की कश्मीर नीति का विरोध करना था. इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुए. इसमें जनता को अच्छा या बुरा में किसी एक को नहीं चुनना था, बल्कि यह तय करना था कि आपातकाल का विरोध किसने किया. आपातकाल से जनता में गुस्सा था. इसका असर चुनाव नतीजों पर भी दिखा. इंदिरा गांधी चुनाव हार गईं. आमतौर पर वही लोग या नेता चुनाव जीते, जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था या जेल गए थे. कई विचारधाराओं और छोटे-छोटे दलों को मिला कर जनता पार्टी नाम से नई पार्टी बनी. जनता पार्टी में जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसे 10 से ज्यादा दल शामिल थे. 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की. कांग्रेस 154 सीटों पर सिमट गई. जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने. हालांकि दो साल में ही गठबंधन सरकार में दरार पड़ने लगी. चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे. 1979 में मोरारजी ने इस्तीफा दे दिया. उनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए. लेकिन इस पद पर वह 6 महीने भी नहीं रह सके. आखिरकार 1980 में जनता पार्टी की ये सरकार गिर गई. 1980 में लोकसभा चुनाव हुए. जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया. लेकिन चुनाव में जनता पार्टी मात्र 31 सीट ही जीत सकी. कांग्रेस ने वापसी करते हुए 350 से अधिक सीटें जीतीं. 1980 से 1989 तक सब ठीक रहा. कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बनी रही. लेकिन 1989 में संयुक्त मोर्चा बना. वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने. ये सरकार सिर्फ 11 महीने ही चल सकी. वीपी सिंह की सरकार इसलिए गिर गई, क्योंकि भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया. इसके बाद 10 नवंबर 1990 को कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने. चंद्रशेखर 21 जून 1991 तक ही प्रधानमंत्री रह सके. फिर पीवी नरसिंह राव की अगुआई में स्थाई सरकार बनी. जिसने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया. मई 1996 में चुनाव हुए. इसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी. अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा. इन चुनावों में जनता दल ने 46 सीटें जीती थी. कई पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया. इसे कांग्रेस ने भी समर्थन दिया. एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के बाद 10 महीने में ये सरकार गिर गई. देवेगौड़ा के बाद इंद्रकुमार गुजराल जनता दल के नेता चुने गए. कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने. लेकिन वो भी एक साल पूरा नहीं पाए और ये सरकार भी गिर गई. 1998 के चुनाव से पहले भाजपा की अगुआई में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना. शुरुआत में इसमें 13 पार्टियां शामिल थीं. 1998 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों ने 258 सीटों पर जीत हासिल की. इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेई प्रधानमंत्री बने.फिर 1999 में आम चुनाव हुए. इसमें एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी. इस सरकार में 24 पार्टियां शामिल थीं. अटल बिहारी वाजपेई प्रधनानंत्री बने. भारत में ये पहली गठबंधन सरकार थी, जिसने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया. 2004 में लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बना. इसकी अगुआई कांग्रेस कर रही थी. उस साल हुए चुनाव में यूपीए ने 222 सीटें जीती थीं. 2009 में फिर मुकाबला एनडीए बनाम यूपीए में हुआ. 2014 में एनडीए और यूपीए का मुकाबला हुआ. हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुआई में भाजपा ने 282 सीटें जीतीं. 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगभग दो तिहाई बहुमत मिला. [wpse_comments_template]

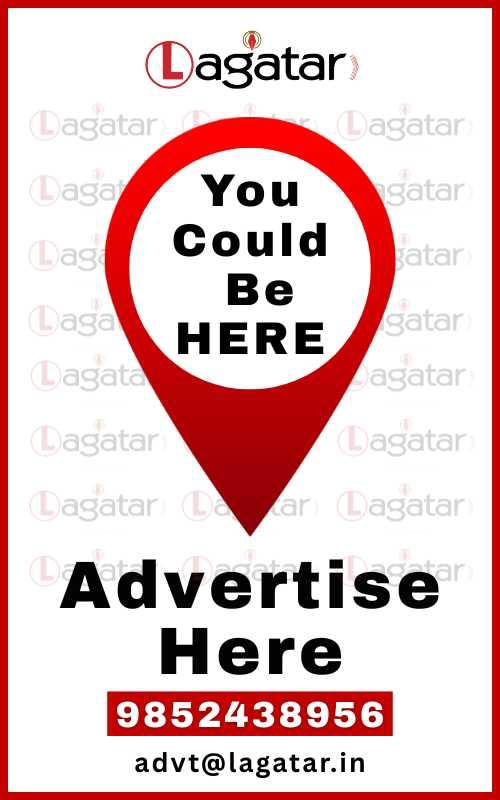
Leave a Comment