2024 के चुनाव की अहमियत

Dr. Pramod Pathak अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं. वैसे तो यह एक स्वाभाविक वैधानिक प्रक्रिया है. किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए और इसमें कोई बहुत बड़ी बहस चलाने की आवश्यकता नहीं. किंतु इस बार के चुनाव शायद बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं. भारत के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के भविष्य के लिए और भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए. इसका अंदाजा हाल फिलहाल की राजनैतिक गतिविधियों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और विपक्ष की तमाम पार्टियों की बेचैनी की वजह यही है. मजे की बात यह है कि विपक्ष से ज्यादा बेचैनी भाजपा के खेमे में दिखाई पड़ रही है. विपक्ष की बेचैनी तो समझ में आने वाली बात है क्योंकि 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कोई भी राजनीतिक गठबंधन या संगठन सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी. इस लिहाज से विपक्ष के खेमे में कम घबराहट दिख रही है. यहां तक कि कांग्रेस में भी, जबकि कांग्रेस आज भी अपने को सत्ता चलाने के लिए सबसे उपयुक्त पार्टी मानती है. किंतु 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा की घबराहट यह संकेत दे रही है कि उनमें सत्ता खोने का भय कहीं ज्यादा है. भले ही उनके शीर्ष नेता बार बार यह कहें कि वह जीत के प्रति पूरी तरह से आशान्वित हैं, उनके अन्दर कि आशंका दिख जाती है. यह राजनीतिक विश्लेषण से ज्यादा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विषय है. सत्ता जाने का भय वैसे तो एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन जब यह चिंता अत्यधिक हो जाए तो कुछ और ही कहानी कहती है. ऐसी परिस्थिति में सत्ता पर काबिज पार्टियां या लोग येन केन प्रकारेण सत्ता पर टिके रहना चाहते हैं. यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है. अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी चरण में यही बेचैनी और आशंका दिखने लगी थी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी वर्ष 74-75 में इसी तरह की बेचैनी और आशंका ने आपातकाल लगाने को प्रेरित किया था. वैसे इमरजेंसी के बाद वर्ष 77 के लोकसभा चुनाव के परिणाम अब किसी भी राजनीतिक दल को उस दिशा में जाने से पहले कई बार सोचने को बाध्य करेंगे. मगर वह सवाल फिलहाल मायने नहीं रखता. आज का प्रश्न तो यह है कि क्या सत्ता के प्रति इतना ज्यादा आसक्त होना लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है? साथ ही एक दूसरा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है. क्या यह प्रवृत्ति स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? राजनीति में मूल्यों की सबसे ज्यादा दुहाई देने वाले आज राजनीति का ही अवमूल्यन कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि देश के बड़े राजनीतिक दल जनतांत्रिक भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं. जनता किसी और पार्टी को चुनती है और पार्टियां उस भावना का सम्मान न करते हुए गलत तरीकों से जोड़-तोड़ की राजनीति कर अपनी सरकार बना लेती हैं. यह प्रक्रिया अब ज्यादा तेज हो गई है. यह चलन लोकतंत्र के भविष्य के लिए ठीक नहीं. यह जन भावना का अनादर है और इससे तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ती है. लोकसभा के वर्ष 1989 के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे. लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 195 सीटें जीत कर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस अन्य पार्टियों से काफी आगे थी. उस समय कांग्रेस के नेता राजीव गांधी थे. दूरदर्शन पर उनसे साक्षात्कार के दौरान पूछा गया कि क्या वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? राजीव गांधी ने बड़े ही स्पष्ट और बेबाक ढंग से कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव के परिणाम यह बताते हैं कि जनादेश उनके खिलाफ है. स्वस्थ लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए इस तरह की परंपरा का निर्वाह करना आवश्यक होता है. दरअसल लोकतंत्र कुछ बुनियादी मूल्यों पर आधारित व्यवस्था है और यदि उनका अनुपालन न किया जाए, तो लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाती है. यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आज हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल्यों का क्षरण हुआ है, अवमूल्यन हुआ है और सत्ता पाने या उस पर काबिज रहने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति का एक साधन बनकर रह गया है. किसी भी तरह सत्ता मिले, कितने भी समय के लिए सत्ता मिले, लेकिन मिले. सोचने वाली बात यह है कि दो महीने, चार महीने, छः महीने के लिए भी लोग सत्ता पर क्यों काबिज होना चाहते हैं. जाहिर है, तात्कालिक स्वार्थ की पूर्ति और लाभ के अलावा इसका कोई अन्य बड़ा कारण तो होगा नहीं. अब प्रश्न यह है कि आखिर इस बदलती हुई राजनीति के लिए दोषी कौन है? समाज की बदलती सोच, लोगों की चेतना में नैतिकता का अवमूल्यन, राजनीति से जुड़े लोगों में बढ़ती स्वार्थ सिद्धि की लालसा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के चरित्र में गिरावट. यह एक चौतरफा क्षरण है, जिसे रोकने का प्रयास आवश्यक होगा. अन्यथा लोकतंत्र विघटित होकर तानाशाही में बदल जाएगा. सहस्राब्दी के सबसे बड़े महानायक के रूप में स्थापित महात्मा गांधी ने सात जघन्य सामाजिक पापों का जिक्र किया था. उनमें से एक था, मूल्य विहीन राजनीति. समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव संभवतः इसी का पड़ता है. वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि यह राजनीति में हमेशा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजनीति को बेहतर बनाने की कोशिश न की जाये. मूल्य तो राजनीति में पहले भी थे तो राजनीति में मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश होनी चाहिए और शायद यही सही समय है. देश बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सिर्फ राजनीतिज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं.


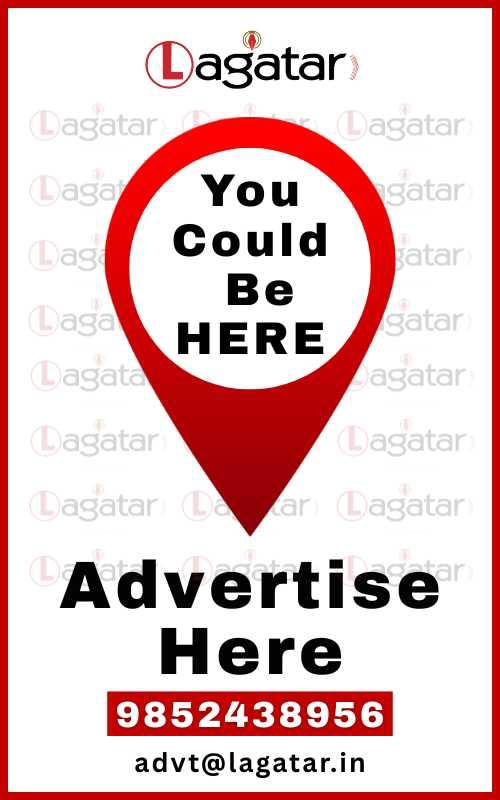
Leave a Comment