Faisal Anurag पच्चीस साल पहले डॉ बीडी शर्मा ने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका शीर्षक था ``हिल उठा हिमालय``. यह पुस्तिका आदिवासियों के स्वशासन के किसी धर्मग्रंथ की तरह लोकप्रिय बन गया था. डॉ शर्मा के प्रयासों का ही नतीजा था कि पेसा एक्ट अस्तित्व में आया. इस पुस्तिका में आदिवासी स्वशासन के एक बड़े मकसद और सपने को दर्ज किया गया था. झारखंड सहित देश भर के हजारों आदिवासी गांवों में एक नारा लोकप्रिय बन कर उभरा था `` हमारे गांव में हमारा राज``. लेकिन इस नारे की हकीकत क्या है. यदि इसे समझना हो तो यह देखना चाहिए कि झारखंड सहित 10 राज्यों की सरकारें पेसा को उसकी मूलभावना के साथ लागू करने की दिशा में कितनी तत्पर रहीं हैं. तत्परता और प्रतिबद्धता का तो हाल यह है कि झारखंड विधानसभा में सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि राज्य में पेसा की नियमावली नहीं बनी है. आखिर नियमावली बनने की राह में बाधा क्या है. यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिससे हर राजनीतिक दल और उसके नेता बचने का प्रयास करते हैं, या सवाल को नजरअंदाज कर देते हैं. नेताओं की एक बाध्यता यह है कि वह आलाकमान को नाराज नहीं करना चाहते जो कि आदिवासी हितों के दावे तो करते हैं, लेकिन अधिकार देने से कतराते हैं. आदिवासी इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी के लिए कॉरपारेट हितों का ध्यान रखने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए स्वशासन एक बड़ा खतरा नजर आता है. जिस तरह भूमि अधिकार कानून और वनाधिकार कानून होने के बावजूद आदिवासियों को अधिकारों के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है. झारखंड में भी जिस तरह लैंड बैंक बनाने के प्रयास में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम तक की परवाह नहीं की गई. आदिवासी इलाकों में प्रॉपर्टी कार्ड के विरोध का सवाल भी इसी स्वशासन से जुड़ा एक अहम मामला है. इसे भी पढ़ें- बिहार">https://lagatar.in/education-became-expensive-in-government-schools-of-bihar-fees-increased-by-two-and-a-half-times/">बिहार
के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई, ढाई गुना तक बढ़ी फीस पेसा नियमावली बनाने की मांग करने वाले आदिवासी समूहों की दो बड़ी मांगें हैं. एक तो यह है कि अनुसूचित इलाकों में सामान्य पंचायती राज को नहीं थोपा जाए और दूसरा यह कि पेसा एक्ट के साथ पंचायती एक्ट का घालमेल नहीं किया जाये. विक्टर मालतो रिजर्व बैंक के बड़े अधिकारी रहे हैं. विक्टर मालतो कहते रहे हैं कि अनुसूचित इलाकों में पंचायती राज का कानून असंवैधानिक है. इसके लिए वे संविधान और पंचायती राज विस्तार अधिनियम का हवाला देते रहे हैं. पेसा कानून बनने के पहले भूरिया कमेटी ने केंद्र को जो रिपोर्ट दी थी उसमें आदिवासी स्वशासन का एक मुकम्मल खाका पेश किया गया था. इसमें पांचवीं अनुसूची वाले इलाकों में भी छठी अनुसूची वाले इलाकों की तरह जिला काउंसिल बनाने का सुझाव दिया गया था. पेसा इस पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहता लेकिन आदिवासी स्वशासन के संवैधानिक संघर्ष करने वाले समूहों का मानना है कि झारखंड सरकार को इस के लिए ठोस पहल करते हुए पेसा को और ज्यादा समग्रता के साथ लागू करने के प्रावधानों को तुरत बनाना चाहिए. हाल ही में रांची में पेसा के रजत जयंती संवाद में कहा गया कि पेसा के एक्ट का निर्माण नहीं करने का मतलब है कि पच्चीस सालों से जारी आदिवासियों के अधिकार हनन की प्रवृति के खिलाफ सरकार कदम नहीं उठा रही है. वक्त आ गया है कि आदिवासी इलाकों को आंतरिक उपनिवेश समझने के बजाय अधिकारों का सम्मान किया जाये. जिस तरह निजीकरण की आंधी देश में चल रहीं है. उसका सीधा असर आदिवासियों के प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ रहा है. इससे आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्र में संवैधानिक गारंटी की हिफाजत करने की दिशा में कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. पेसा के बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि प्राकृतिक संसाधनों, लघु वनोपज और लघु खनिज के प्रबंधन के पूरे अधिकार ग्राम सभाओं को दिये जाएंगे. लेकिन ग्रामसभा के नाम पर भी देखा गया हे कि उसका किस तरह मजाक बनाया जाता रहा है. ग्राम सभाओं को सशक्त और निर्णायक बनाने के बजाय उसे स्थानीय प्रशासन के भरोसे ही छोड़ दिया गया है. दरअसल, आदिवासी स्वशासन एक भिन्न दृष्टिकोण की मांग करता है. न ही पेसा और न ही आदिवासी स्वशासन का सवाल केवल एक प्रशासनिक मॉडल भर है. बल्कि वह एक सांस्कृतिक विशेषताओं के समायोजन और संरक्षण के व्यापक आदिवासी चेतना का हिस्सा भी है. इसे भी पढ़ें- रितेश">https://lagatar.in/shocking-disclosure-of-ritesh-not-yet-married-to-rakhi-sawant/">रितेश
का शॉकिंग खुलासा, कहा-राखी सावंत से अभी तक नहीं की शादी, मन का है रिश्ता पच्चीस साल पहले पीए संगमा लोकसभा के अध्यक्ष थे और केंद्र में एक संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसने पेसा बनाया. तब देश में नवउदावादी आर्थिक नीतियों को लेकर भारी असंतोष था. और भारतीय राजनीति भी मंडल बनाम मंदिर के विवाद में बिखरी थी. देश में के तमाम कमजोर तबकों में एक उभार हो रहा था. मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद राजनीति पूरी तरह बदल रही थी. 1991 में नरसिंह राव और मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के सवाल पर देश में भारी विरोध भी था. यही नहीं डंकल प्रस्तावों के गर्भ से निकले विश्व व्यापार संगठन भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हुआ था और विश्व भर में उभरे आदिवासी आंदोलनों से भारत में भी एक नयी लहर पैदा हुई थी. लेकिन पच्चीस सालों में राजनीति पूरी तरह बदल गयी है और आर्थिक सुधारों के केंद्र में कमजोर वर्ग के हित नहीं रह गए हैं. देशी-विदेशी बहुराष्ट्रीय निगम सरकारों पर भी प्रभावी हैं. ऐसे में आदिवासी स्वशासन का टकराव सीधे इन्हीं ताकतों के साथ है. देखना है कि विधानसभा में राज्य सरकार की स्वीकारोक्ति के बावजूद पेसा नियामावली की राह में खेड़े अवरोध हटते हैं या नहीं. इसे भी पढ़ें-होते">https://lagatar.in/we-are-becoming-poor-and-poor-but-pretend-that-we-becoming-a-superpower/">होते
जा रहे हैं कंगाल-बदहाल, दिखावा ऐसा कि महाशक्ति बन रहे [wpse_comments_template]

क्या सपना ही बना रह जाएगा आदिवासी स्वशासन


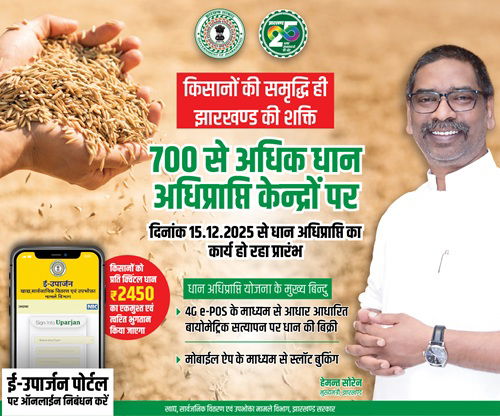

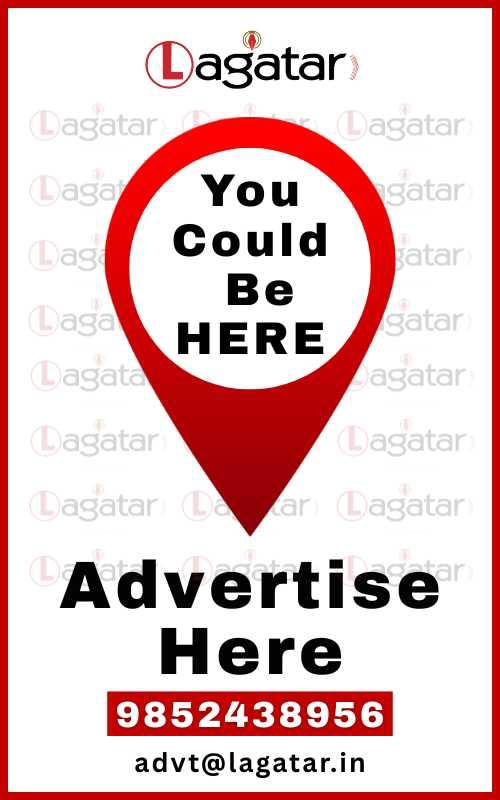
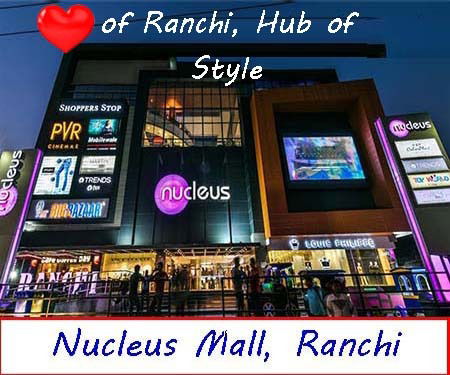
Leave a Comment